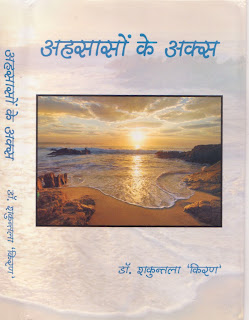रविवार, 29 जनवरी 2012
मंगलवार, 5 जुलाई 2011
स्त्री विमर्श की कसौटी परः मीरांबाई और उनकी कविता
स्त्री विमर्श की कसौटी पर : मीरांबाई और उनकी कविता
-अर्पणा दीप्ति
डॉ.हेमा रंगन की समीक्षाकृति "संत मीरांबाई का रचना संसारः एक स्त्रीवादी विमर्श" [2011 ] निस्संदेह अत्यंत महत्वशाली शोधपूर्ण कृति है।इसमें लेखिका ने इस आधारभूत प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है कि 'मीरां क्या केवल एक संत,एक भक्त या प्रेयसी भर थी , या फिर हाड़ मांस की बनी एक साधारण स्त्री जिसने सामाजिक रीति रिवाजों को चुनौती दी थी?' वस्तुतः वे भक्त, कवयित्री या संत जो भी बनीं उस सबसे पहले स्त्री थीं जिनके साथ पितृसत्तात्मक सामंतवादी समाज ने दोयम दर्जे का व्यवहार किया ।
कबीर और मीरां मध्यकाल के दो तेजस्वी व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनकर बाह्यजगत की वर्जनाओं को लांघा। कबीर पुरुष थे इसलिए बहुत हद तक सामाजिक प्रताड़नाओं से बच गए। लेकिन मीरां स्त्री थीं अतः प्रताड़नाओं से बचने का उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने जुझारू व्यक्तित्व के बल पर ही वे समस्त बाधाओं को पार करती स्वतंत्र मानवी बन सकीं।
हेमा रंगन नें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीरां के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर मीरां के जीवन के छुए एवं अनछुए पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है।लेखिका का यह प्रयास एक स्त्री के सम्मान, उसकी आंतरिक शक्ति एवं संघर्षरत व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए समूचे स्त्री समाज की संघर्ष गाथा का प्रतिनिधित्व करता है। लेखिका ने भारतीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का प्रतिबिंब रही मीरां को स्त्रीवादी तथ्यों के आधार पर स्त्री विमर्श का मुद्दा बनाया है।
मध्यकाल में सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा बड़ी ही सोचनीय थी। समाज के सभी तबकों में बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी। लड़की को शिक्षित करने का प्रचलन नहीं था, गृहकार्य में कुशलता प्राप्त करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। बहुविवाह की परंपरा ने स्त्रियों की स्थिति को दयनीय बना दिया था । सौतिया डाह कभी-कभी पति तथा सौतेले पुत्रों की जान लेने की सीमा तक पहुँच जाता था । पुरुषों ने सौंदर्योपासना तथा विलास के सभी द्वार अपने लिए खोल रखे थे किंतु स्त्रियों के लिए पतिनिष्ठा और यौनशुचिता अनिवार्य थी। सती-प्रथा और जौहर की राजस्थान में एक खास परंपरा रही है किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है ये प्रथाएँ केवल स्त्रियों के लिए ही अनिवार्य थीं । पुरुष अनेक स्त्रियों को पत्नी और रखैल बनाकर रख सकता था लेकिन स्त्री का एक ही पति हो सकता था जिसके मरते ही उसे उसके साथ चिता में जला दिया जाता था। पति के जीवनकाल में पतिपरायणता तो ठीक,लेकिन पति के मरणोपरांत ’सहमरण’ या ’अनुमरण’ द्वारा निष्ठा साबित करने का कोई औचित्य नहीं। किंतु इसका एक और पहलू भी हो सकता है।उस समय के समाज में विधवा की जो दुर्दशा थी उसे लंबे समय तक तिल-तिल कर झेलने के बजाए एक बार में शरीर को आग के हवाले करना शायद कम कष्टप्रद रहा होगा। इसी प्रकार जौहर प्रथा को राजपुतानी आन का प्रतीक माना जाता था।क्रूर मुसलमान आक्रमणकारियों से अपनी स्त्रियों को बचाने का यही एक आखिरी रास्ता था । अग्नि प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से स्त्रियों तथा लड़कियों द्वारा आत्मदाह करना या फिर परिवार के पुरुषों द्वारा शत्रुओं के बीच युद्ध करने से पूर्व उन्हें आग के हबाले कर देना। किन्तु यह प्रश्न भी यहाँ उठना लाजिमी है कि मुगलो ने तो समस्त भारत को अपने अधीन किया, फिर यह प्रथा समूचे हिंदुस्तान में प्रचलित क्यों नहीं हुई? इन सब प्रश्नों से टकराते हुए लेखिका ने मीरां के जीवन और व्यक्तित्व संबंधी तथ्यों की विस्तार से पड़ताल की है।
मान्यता है कि मीरां का एक भाई था जो नहीं रहा। पिता भी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। मीरां के संरक्षण का जिम्मा उसके चाचा राव वीरमदेव पर आ गया । मीरां ने बचपन में जो कुछ खोया उस सवकी क्षतिपूर्ति के रूप में ’गिरिधर नागर’ को पा लिया। 11-12 वर्ष की अवस्था में मीरां का विवाह मेवाड़ के ’हिंदू धर्म सूर्य’ महाराणा संग्रामसिंह के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 में हुआ । ससुराल में आते ही स्वतंत्र व्यक्तित्व में आस्था रखने वाली मीरां ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार करते हुए अपने आराध्य ’गिरिधर नागर’ की पूजा प्रारंभ कर दी। पति भोजराज मीरां के व्यवहार से क्षुब्ध हुए, उनके मन में अनेक प्रकार की शंकाए उठीं जो बाद में शांत हो गईं । मीरां की संतान का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; शायद पति से मीरा का समागम न हुआ हो। ससुरालवालों का मानना था, मीरां ’कुलबोरनी’ तथा ’लोकलाज बिसारने’ वाली है। लोक मान्यता के अनुसार कुँवर भोजराज की मृत्यु 1528 में राणा सांगा के जीवन काल में हो गई थी। मीरां का वैवाहिक जीवन मुश्किल से दस वर्ष रहा। राणा सांगा के बाद रतनसिंह मेवाड़ का राजा बना । मेवाड़ की परंपरा के अनुसार उसने मीरां को सती होने का आदेश दिया । मीरां ने कभी लौकिक जीवन में भोजराज को अपना पति नहीं माना तो अपने आपको उसकी विधवा कैसे मान सकती थी! उसका विवाह तो बालपन में ही ’गिरिधर गोपाल’ से हुआ था जो अविनाशी थे,यों वह तो चिर सुहागन थी -
"जग सुहाग मिथ्या री सजनी, होवां ही मिट जासी।/
गिरिधर गास्यां , सती न होस्यां मन मोहयो घनघामी॥"
"लोग कहयां मीरां भई बाबरी, सासू कहयां कुलनाशी ।"
मीरां ने रतनसिंह के आदेश को ठुकरा दिया। फिर क्या था! मीरां पर अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता ही गया। चरणामृत के नाम पर विष और शालिग्राम की मूर्ति के नाम पर विषैला नाग भेजा गया। इन अत्याचारों से तंग आकर सन 1534 के आसपास मीरां मेवाड़ त्यागकर मेडता चली गई । जनश्रुतियों के अनुसार मीरां वृंदावन गई। जीवन के अंतिम पड़ाव में गुजरात का द्वारका मीरां का निवास स्थान रहा।
1888 में कर्नल टॉड ने प्रामाणिक दस्तावेजों के अभाव में किंवदंतियों का सहारा लेकर राजस्थान के समग्र इतिहास पर केंद्रित पुस्तक ’एनल्स एंडेंटिक्वटीज आफ राजस्थान’ लिखी। इसमें मीरां को महाराणा कुंभा की पत्नी बताया गया। टॉड की इस मान्यता को विद्वानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। डॉ.सी.एल.प्रभात के अनुसार मीरां के गुरु शायद रैदास या रैदासी रहे होंगे। किंतु पुनः विभिन्न धर्म संप्रदायों का अध्ययन करने पर डॉ.प्रभात इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मीरां का कोई एक दीक्षा गुरू नहीं रहा होगा। मीरां के ही शब्दों में ’मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।’ पद्मावत शबनम ने ’मीरां : व्यक्तित्व एवं कृतित्व’ में यह दर्शाया है कि सरकारी तौर पर जो मीरां की प्रामाणिक तस्वीर है वह राजस्थानी विधवा की नहीं है, न ही राजसी है - गले में तुलसी माला किंतु कलाइयों में चूड़ियाँ हैं। भजन में मग्न सादगीपूर्ण यह चित्र भक्त स्त्री का है न कि विधवा का। इन सभी विद्वानों के विवरण का अध्ययन करने पर एक प्रश्न उभरकर सामने आता है - आर्थिक आधार का प्रश्न।
इसके अतिरिक्त लेखिका ने मीरां की भक्ति साधना पर निर्गुण तथा सगुण भक्ति के प्रभाव को भी दर्शाया है। मीरां सगुण उपासिका तथा कृष्ण की भक्त थीं। लेकिन उनकी इस उपासना पर नाथ मत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है-
"म्हारे घर रमतो ही आई रे जोगिया।/काना बिच कुंडल,गले बिच सेली, अंग भभूत रमाई रे ।"
वहीं संत मत का प्रभाव भी द्रष्टव्य है-
"राम नाम रस पीजै!/
मनवा! राम नाम रस पीजै/
तजि कुसंग सतसंग बैठि हरि चरचा सुनि लीजै/
काम क्रोध मद मोह लोभ कू, चित से बहाय दीजै/
मीरां के प्रभु गिरिधर नागर,ताके रंग में भीजै।"
मीरां की कुछ मार्मिक पंक्तियों में संतो का फक्कड़पना तथा सूफ़ियों की दीवानगी दिखाई देती है-
"हेरी मैं तो दरद दिवाणी मेरो दरद न जाने कोई/
घाइल की घाइल जाणै कि जिन लाइं होई॥"
मीरां ने राम भक्ति के पद न के बराबर गाए किंतु मीरा के पदों में राम का उल्लेख अनेक रुपों में बार-बार आया है-
"मैंने राम रतन धन पायो/
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करि किरपा अपनायो।"
मीरां की कृष्ण भक्ति के स्वरूप की मुख्य विशेषता लेखिका के अनुसार यह है कि न तो वह गोपी है और न राधा है, वह सौ फीसदी मीरां है तथा अपने गिरिधर नागर से उसका सीधा संबंध है।
मीरां के काव्य विषयों का वर्गीकरण करते हुए लेखिका ने मीरां के आराध्य, मीरां की साधना के स्वरूप और मीरां के भावजगत का मनोवैजानिक विश्लेषण भी किया है। इस विश्लेषण से एक बात स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने आती है कि मीरां ने ’स्त्री-मुक्ति’ का सूत्रपात ही नहीं किया अपितु अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अस्तित्व की बाजी लगाकर उसने स्त्री के मान सम्मान को बढ़ाया। अतः उसे ’स्त्री-स्वतंत्रता’ का सूत्रपात करनेवाली प्रथम वीरांगना माना जाना चाहिए।
आगे मीरां के साहित्य का भाषिक विश्लेषण करते हुए दर्शाया गया है कि मीरां ने भाषा को कलात्मक विशिष्टताएँ देने का प्रयास कतई नहीं किया, न ही काव्यशास्त्रीय नियमों का कड़ाई से पालन किया। मीरां के फुटकर पद साधारण लोकगीतों की तरह बोलचाल की भाषा में हैं लेकिन इन पदों में शृंगार, मधुर तथा शांत रस के पदों की प्रचुरता आसानी से देखी जा सकती है।
अंत में लेखिका ने हिंदी गीति पंरपरा में कबीर, रैदास, सूरदास और तुलसीदास के साथ मीरां की तुलना करते हुए मीरां को इन सबमें सबसे ऊपर स्थान दिया है। भारतीय संगीत-संपदा को समृद्ध करने में मीरां के पदों का योगदान अतुलनीय है। कुल मिलाकर यह कहना सर्वथा संगत होगा कि डॉ.हेमा रंगन ने अपनी इस कृति द्वारा मीरां के स्त्री रूप की प्रतिष्ठा की है और स्त्री विमर्श के भारतीय संदर्भ का सूत्रपात करने में उनकी भूमिका का सप्रमाण प्रतिपादन किया है।
समीक्षित कृति - संत मीरांबाई का रचना संसार :एक स्त्रीवादी विमर्श
लेखिका - डॉ.हेमा रंगन
संस्करण - जनवरी 2011
प्रकाशक - शुभंकर प्रकाशन, रामकुंज, आर के वैद्य रोड,दादर,मुंबई-400028
पृष्ठ संख्या- 315
मूल्य - 250रुपये मात्र.
बुधवार, 22 जून 2011
फूले कदम्ब
फूले कदम्ब
टहनी -टहनी में कंदुक सम झूले कदम्ब
फूले कदम्ब |
सावन बीता
बादल का कोप नहीं रीता
जाने कब से तू बरस रहा
ललचाई आँखों से नाहक
जाने कब से तू तरस रहा
मन कहता है, छू ले कदम्ब
फूले कदम्ब
फूले कदम्ब
नागार्जुन
गुरुवार, 14 अप्रैल 2011
सहजता में गहराई: 'अहसासों के अक्स'
डॉ.शकुंतला किरण की पुस्तक ’अहसासों के अक्स’ 108 कविताओं का संकलन है। कवयित्री ने अपनी इन कविताओं में जहाँ एक ओर वर्तमान मानव समाज में उपजी विसंगतियों एंव विकृतियों को अर्थपूर्ण स्वर प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर भक्ति गीतों के माध्यम से कोमल पक्षों को भी उजागर किया है। शकुंतला किरण का काव्य संग्रह चार खंडो में विभाजित है। पहला खंड गीत, दूसरा राजस्थानी कविताएँ,तीसरा अतुकांत कविताएँ और अंतिम भक्ति गीत। अपनी बात में कवयित्री स्वयं यह कहती नजर आती हैं कि-"निरंतर मूल्यविहीन होते जा रहे सामाजिक सरोकार, मानवीय-संबंधों की असहज व बोझिल होती जटिल संवेदनाएँ, राजनीतिक परिदृश्य पर उभरी विद्रूपताएँ आदि के प्रति आक्रोश की धधकती ज्वाला, मन के किसी कोने में दुबके छुपे काव्यबोध को जगाकर प्रेरित करने लगी, फलस्वरूप कुछ गीत/ कविताओं ने जन्म लिया ।" इन काव्य संग्रह को पढ़ने से ऎसा प्रतीत होता है कवयित्री मूलतः गीतकार है। उनके गीतों में पीड़ा है,अकुलाहट है,यही अकुलाहट उन्हें कवि बनाती है-
" घावों का सागर अति गहरा,/सपनों पर विरहा का पहरा,/ फिर विरहिन के नयनों में यह-/ निंदिया क्यों घिर आई ।"
(मुक्ति थी जिसके बंधंन में....पृ.सं.19)
पुस्तक का प्रारभं दोहों से किया गया है। यहाँ एक प्रश्नाकुल मन की बेचैनी देखी जा सकती है -
"शब्द तुम्हारे दे रहे, यूँ अब भी अधिकार।/अर्थ दूर क्यों जा बसे, सात समन्दर पार ॥"
(अर्थ दूर क्यों जा बसे....पृ.सं.11)
जहाँ एक तरफ कवयित्री व्यथित हैं वहीं दूसरी ओर जीवन के प्रति आस्थावान भी हैं।जिस प्रकार पतझड़ और वसंत का आना-जाना सृष्टि का चक्र है ठीक उसी प्रकार सुख और दुख का आना-जाना मनुष्य के जीवन का चक्र है। शकुंतला किरण ने सृष्टि तथा जीवन के इस शाश्वत नियम को बड़े सहज भाव से अपने इस गीत में दर्शाया है -
"रिसने दो आँसू को, पीड़ा की आँख तुम,/फागुन की मस्ती से आओ, हम परिचय कर लें/ ........./ केसर और टेसू के, रंगों में भीग-भीग,/ इठलाती-सुधियों का आओ, हम संचय कर लें।"(बजने दो चंग....पृ.सं.16)
प्रकृति और मनुष्य का संबंध आदिकाल से रहा है । शकुंतला किरण ने अपने गीतों में इस परंपरा का निर्वाह बखुबी किया है। बड़ी सहजता के साथ उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है-
"सपन की पुष्प देहरी पर,खिली है चाँदनी जब से,/सुरों की सरगमी-फागुन,सुनाये रागिनी जब से,/ फुहारों की छुअन सुखे अधरों पर लिख गई सावन/ हर इक पल हो गया ऋतुराज गंधित यामिनी जब से।" (सपन की पुष्प देहरी पर....पृ.सं.45)
आदमी चाहे विदेश में क्यों न हो वह अपनी मातृभाषा का मोह नही छोड़ पाता । शकुंतला किरण के राजस्थानी गीतों में मातृभाषा का यह मोह बड़े ही स्पष्ट एंव सरस रूप में दिखाई देता है। कहीं सास जँवाई को सीख देती नजर आती है तो कहीं बहुएँ सास-पुराण सुनाती दिखाई पड़ती है। ’कवि सम्मेलन री झाँकी’ तथा ’पाणीवाड़ा री झाँकी’आदि गीत भी हँसकर लोट-पोट होने पर विवश करते हैं। इन गीतों में हास्य-व्यंग्य की प्रधानता है यथा-
"सुनो कवँरसा बाई नै म्हे, घणा लाड़ सू पाली पोसी।/भोली डारी छोरी म्हाँरी, सब बातां मे है संतोषी॥/सव कामां में तेज घणी, आ पण गुस्सा की है खारी।/थे मत बहस बराबर कर जो, कवँर साब आ विनती म्हारी॥" (सासू री सीख-जवाँई रे नाम पृ.सं.50)
अतुकान्त कविता की शृंखला में कवयित्री ने मूल्यविहीन होते हुए समाज,स्त्रियों की दयनीय स्थिति तथा मानव संबंधों को उकेरा है-
"इन जर्जर संबंधो में-/ अपनत्व खोजना/ठीक वैसा ही है-/ जैसे शवों में स्पंदन की चाह।" (संबंध-पृ.सं.-61)
स्त्रियों के चहुँमुखी शोषण एवं उनकी पराधीनता पर कवयित्री दुखी हैं । नारी विषयक विकृतियों एवं उनकी स्वतंत्रता का हनन करने वाले सभ्य समाज पर ‘अभिशप्त ’ कविता के माध्यम से कवयित्री ने जमकर प्रहार किया है-
"मैं/भेड़ों के झुण्ड से-/निकल भागने का /विद्रोह नहीं/ सिर्फ कुछ स्वतंत्रता से-/आगे-पीछे,/बिना किसी से सटे/चलना चाहती हूँ!/ ले..कि...न/ तुम्हारी कर्कश हाँक,/और लकड़ी,/बार-बार/झुण्ड में मिलकर,/सबसे सटकर,/ चलने को विवश कर देती है!/ यह कैसी नियति है! (अभिशप्त-पृ.सं.69)
कहने को तो हम आज स्त्री सशक्तीकरण की दौड़ में शामिल है। लेकिन क्या कामकाजी महिलाएँ घर के बाहर सुरक्षित है ? इस प्रश्न को कवयित्री ने ‘अंह की तुष्टि ’ में बड़ी ही सशक्त मुद्रा से उठाया है-
"चारो ओर बैठे हुए दैत्य/निगाहों में नाखुनों-/और अनर्गल प्रश्नो के चाकू से,/किसी मासुम व्यक्तित्व के चिथड़े-चिथड़े उड़ा,/उसे नंगा कर,/ अपने अहं की तुष्टि पर-/ठ....हा....के लगा रहे हैं।" (अहं की तुष्टि-पृ.सं.-74)
बदलते मूल्य, खंडित होते विश्वास एवं प्रगतिशील समाज में दहेज रूपी दानव ने आज भी कितनी ही लड़कियों को मौत की गोद में सुला रहा है। आज की शिक्षित युवा पीढ़ी भी दहेज रुपी दानव के चंगुल से मुक्त नही हो पाई है । उनकी तथाकथित मुक्ति केवल भाषण तथा कलम तक ही सीमित है। ‘अलविदा मेरे गुलाब ’ में कवयित्री हृदय को झकझोरने वाले कुछ प्रश्न पाठको के समक्ष रखती हैं-
"एम.ए. की डिग्री,बैंक की क्लर्की,/फिर भी न दहेज में स्कुटर?/न फरमाइश पर मित्रों के लिए शराब?/और इस भयंकर अपमान का बदला,/सिर्फ.....सिर्फ माधुरी की हत्या हीं तो-/हो सकता था!/बधाई लो मनु अपनी इस सफलता पर,/अहं पर /पुरुषार्थ पर,/ और उस स्कूटर व शराब के प्रतिष्ठित सवाल पर !!(अलविदा मेरे गुलाब पृ.सं.-76)
जहाँ एक तरफ स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार से कवयित्री दुखी हैं वहीं दुसरी तरफ उधार में दी गई सुविधाओं के विरुद्ध बगाबत करती हैं-
"विरासत में मिले-/सुविधाओं के पंख,/न मेरे पास है/न उधार लेना चाहती हूँ।" (पंख-पृ.सं.71)
इसी प्रकार शकुंतला किरण मूल्यविहीन राजनीति तथा सत्तालोलु्पों एवं भ्रष्टाचारियों पर भी जमकर प्रहार करने से नहीं चूकती हैं-
"इस बार.../अंधे धृतराष्ट्र के लिए/ गांधारी के साथ ही-/सभी प्रधान गण भी,/आँखों पर पट्टी बाँध,/स्वामी भक्ति में-/कुत्तों से भी आगे बढ़ते रहे!/ बेबस जनता को काटते रहे!" (अंधा राज-पृ.सं.-87)
आज की युवा पीढ़ी संवेदना शून्य तथा हृदयहीन हो चुकी है। संबंधों को भी नफा-नुकसान के तराजु पर तोला जा रहा है। वृद्ध असहाय माता-पिता के प्रति उदासीन होते युवाओं को भी कवयित्री ने जमकर लताड़ा है-
"पद-यात्रा करते-करते,/जब चढाव पर-/श्रवण कुमार की आँखे/रुप और राशि में ही-/ अटक गई,/तो काँवड़ में बैठी माँ,/ अचानक
उलट गई!/झाँका तो पाया कि-/कुँआ बहुत गहरा व अंधा है!/ और सूरज भी-/ साथ देने में,/आनाकानी कर रहा है। " (अप्रत्यशित-पृ.सं.-89)
मार्क्स का सामाजिक समता का सिद्धांत सिर्फ किताबों तक ही सीमित हो चुका है। वर्तमान समाज में अमीरी-गरीबी की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे पाटना नामुमकिन दिखता है। ‘गरीबी की सजा ’ में कवयित्री ने आम आदमी के कुछ ऎसे ही प्रश्न बड़े सहज ढंग से उठाए हैं-
"तुम नहीं जानते!/उनके बड़े-बड़े गुनाहो की उम्र भी,/हमारे छोटे-छोटे गुनाहों से-/बहुत कम होती है।..../अपने गुनाहों के कंबंल को ओढ़ा देते हैं/ठिठुरते गरीब व बेबस लोगों को-/साथ ही उन्हें कारावास में-/मुहैया करवा देते हैं/ दो वक्त की रोटी!" (गरीबी की सजा -पृ.सं.-104)
भक्ति गीतों में कवयित्री कहीं कान्हा के लिए श्रृंगार करती हैं तो कहीं विरहनी राधा बनी भी दृष्टिगोचर होती हैं-
"उद्धव से संदेश तुम्हारे,समझ नहीं हम पाते हैं।/मन तड़पत है आओ कान्हा, आँसू तुम्हे बुलाते हैं।।" (ये आँसू तुम्हे बुलाते हैं....पृ.सं.-104)
शकुंतला किरण की असली शक्ति उनकी गुरुभक्ति है। कवयित्री गुरु को ईश्वर के रूप में महसूस करती हैं-
"तुम ही हो ईश्वर गुरुवर,तुम परम ब्रह्म तुम ज्ञानी।/तुम ही तो ब्रह्मा,विष्णु ,तुम ही शिवशंकर दानी। (है आज गुरु पुनम तुम.....पृ.सं.110)
गुरुभक्ति में सराबोर कवयित्री की गुरु के प्रति समर्पण याचना भी अदभुत है-
"समर्पण निःशेष हो मेरा,तुम्ही आधार हो,/तुमसे तुमको माँगने की याचना स्वीकार हो ।( तुमसे तुमको माँगने की..... पृ.सं.110)
अपने काव्य संग्रह ‘अहसासों के अक्स’ में कवयित्री शकुंतला किरण ने दोहे,गीत,गजल, मुक्तक,राजस्थानी कविता तथा भक्ति गीतों आ के माध्यम से सशक्त काव्य अभिव्यक्ति का परिचय दिया है। कवयित्री की मातृभाषा राजस्थानी में लिखी गई कविताएँ अविस्मरणीय होगीं इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही इसमें कोई संदेह नही कि शकुंतला किरण के भक्तिगीत श्रेष्ठ राजस्थानी परंपरा की रचनाएँ हैं। मीराबाई के पदों की तरह इन गीतों का भी गायन मंदिरों में हो सकता है।
अंततः इस काव्य संग्रह की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सहज भाषा में पर्याप्त गहराई भरी गई है। कवयित्री की काव्य प्रतिभा तथा भक्ति भावना हमेशा बनी रहे , इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशा है कि हिंदी जगत ‘अहसासों के अक्स ’ का स्वागत करेगा ।
- अर्पणा दीप्ति
समीक्षित कृति-अहसासों का अक्स
कवयित्री - डॉ.शकुंतला किरण
प्रकाशक- संकेत प्रकाशन, 372/26,रामगंज,
संस्करण-2009
पृष्ठ संख्या - 152
मूल्य-35o रुपए
सोमवार, 1 नवंबर 2010
मंगलवार, 19 अक्टूबर 2010
जीवन के जमीनी संघर्ष की उपज मुनिला :'माटी कहे कुम्हार से'
|
सदस्यता लें
संदेश (Atom)
गणपति का आगमन
जब से हम हैदराबादी हुए गणपति उत्सव मानों खुशियों का खजाना | खासकर अनुराग बाबू को यह त्योहार सबसे ज्यादा भाता है | अपने छुटपन में बप्पा क...

-
भीष्म साहनी का 2000 ई.प्रकाशित उपन्यास " नीलू नीलिमा नीलोफर " प्रेम कहानी है । इस उपन्यास की कथा वस्तु बाल्यकाल की दो सखियाँ नीलू ...
-
महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक महात्मा तुलसीदास थे। वे युग्स्रष्टा के साथ-साथ युगदृष्टा भी थे। आचार्य हजारी प्रस...
-
अर्पणा दीप्ति यथार्थ मानव जीवन की सच्ची अनुभूति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में घटित होने वाले घटनाओं एवं भावनाओं का अनुभव करते हैं।...